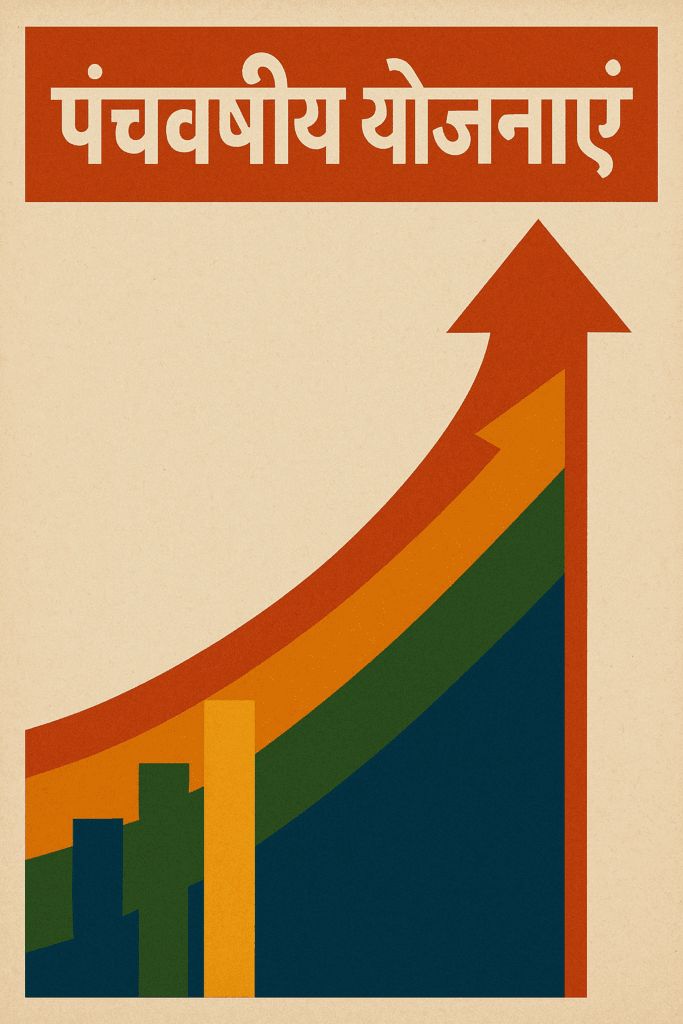🛠 भारत की पंचवर्षीय योजनाएं: विकास की नींव
प्रस्तावना:
भारत जैसे विशाल और विविधताओं वाले देश के लिए सुनियोजित आर्थिक और सामाजिक विकास अत्यंत आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं (Five Year Plans) की शुरुआत की। ये योजनाएं देश की आर्थिक दिशा निर्धारित करने और संसाधनों के बेहतर उपयोग की योजना बनाने के लिए बनाई जाती हैं।
भारत के स्वतंत्र होने के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी—गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन और असमानता जैसी समस्याओं का समाधान। इन समस्याओं के स्थायी समाधान हेतु देश में योजनाबद्ध विकास का निर्णय लिया गया, और पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई।
📜 पंचवर्षीय योजनाओं का इतिहास:
भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत 1951 में हुई थी। यह मॉडल सोवियत संघ (USSR) से प्रेरित था। भारत में अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं।
🧱 प्रमुख पंचवर्षीय योजनाएं:
🔹 पहली पंचवर्षीय योजना (1951-1956)
- मुख्य लक्ष्य: कृषि, सिंचाई और ऊर्जा।
- प्रमुख योगदान: भाखड़ा-नांगल बांध, कृषि उत्पादन में वृद्धि।
🔹 दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-1961)
- मुख्य लक्ष्य: औद्योगिकीकरण।
- नीति निर्माता: पं. जवाहरलाल नेहरू व पी.सी. महालनोबिस।
- प्रभाव: भारी उद्योगों की स्थापना, इस्पात संयंत्रों की शुरुआत।
🔹 तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-1966)
- मुख्य लक्ष्य: आत्मनिर्भरता और खाद्यान्न उत्पादन।
- बाधाएँ: 1962 का चीन युद्ध, 1965 का पाकिस्तान युद्ध और सूखा।
🔹 चौथी से सातवीं योजनाएं (1969-1990)
- प्रमुख विषय: गरीबी हटाओ, रोजगार सृजन, ग्रामीण विकास।
- इंदिरा गांधी के दौर में “गरीबी हटाओ” प्रमुख नारा बना।
🔹 आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-1997)
- महत्वपूर्ण मोड़: आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG नीति) की शुरुआत।
🔹 ग्यारहवीं और बारहवीं योजनाएं (2007-2017)
- मुख्य उद्देश्य: समावेशी विकास (Inclusive Growth), शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार।
प्रमुख पंचवर्षीय योजनाएं और उनका विवरण:
| योजना क्रमांक | अवधि | मुख्य उद्देश्य | प्रमुख उपलब्धियाँ / चुनौतियाँ |
|---|---|---|---|
| 1. पहली योजना | 1951–1956 | कृषि क्षेत्र पर ज़ोर, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना | भाखड़ा नांगल बाँध, सिंचाई परियोजनाएँ |
| 2. दूसरी योजना | 1956–1961 | औद्योगिकीकरण और भारी उद्योग | इस्पात संयंत्र (भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला) |
| 3. तीसरी योजना | 1961–1966 | आत्मनिर्भरता और खाद्य सुरक्षा | चीन युद्ध, सूखा, योजना असफल रही |
| 4. चौथी योजना | 1969–1974 | गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता | ‘गरीबी हटाओ’ नारा, मिश्रित सफलता |
| 5. पाँचवीं योजना | 1974–1979 | गरीबी हटाना, आत्मनिर्भरता | 20 सूत्रीय कार्यक्रम, आपातकाल में बाधा |
| 6. छठी योजना | 1980–1985 | औद्योगिक विकास, रोजगार | हरित क्रांति का विस्तार, सेवा क्षेत्र का विकास |
| 7. सातवीं योजना | 1985–1990 | उत्पादन में वृद्धि, सामाजिक सेवाओं पर ध्यान | ग्रामीण रोजगार योजनाएं, शिक्षा में सुधार |
| 8. आठवीं योजना | 1992–1997 | आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण | LPG नीति, विदेशी निवेश में वृद्धि |
| 9. नौवीं योजना | 1997–2002 | समान विकास, महिला सशक्तिकरण | मानव संसाधन विकास, ग्रामीण योजनाएं |
| 10. दसवीं योजना | 2002–2007 | विकास दर 8% लक्ष्य, सामाजिक न्याय | आईटी सेक्टर में उछाल, गरीबी में कमी |
| 11. ग्यारहवीं योजना | 2007–2012 | समावेशी और सतत विकास | शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण क्षेत्रों पर ज़ोर |
| 12. बारहवीं योजना | 2012–2017 | ‘तेजी से, समावेशी और सतत’ विकास | शिक्षा में सुधार, आधारभूत ढांचा विकास |
🏢 पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत बने प्रमुख संस्थान:
-
भारतीय योजना आयोग (Planning Commission) – 1950 में गठन
-
नीति आयोग (NITI Aayog) – 2015 में योजना आयोग के स्थान पर गठित
-
राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council) – योजनाओं को अनुमोदित करने वाला सर्वोच्च निकाय
📌 पंचवर्षीय योजनाओं की विशेषताएं:
-
लक्ष्य-आधारित योजना: हर योजना का एक विशिष्ट लक्ष्य होता था जैसे गरीबी उन्मूलन, कृषि विकास या औद्योगिक प्रगति।
-
समयबद्ध योजना: हर योजना 5 वर्षों की होती थी।
-
संसाधन प्रबंधन: सीमित संसाधनों का प्रभावशाली उपयोग सुनिश्चित करना।
-
सहकारी संघवाद: केंद्र और राज्य दोनों की सहभागिता से योजनाओं का निर्माण और कार्यान्वयन।
⚠️ चुनौतियाँ:
-
राजनीतिक अस्थिरता के कारण योजनाएं अधूरी रहना।
-
योजना निर्माण और कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार।
-
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच असमान विकास।
-
कई बार योजनाएं आंकड़ों पर आधारित थीं, ज़मीनी सच्चाई से नहीं।
🔚 पंचवर्षीय योजनाओं का अंत:
भारत सरकार ने 2017 में पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया और अब नीति आयोग (NITI Aayog) के माध्यम से लचीलापन भरी और अधिक केंद्रित योजनाएं बनाई जा रही हैं।
📊 निष्कर्ष:
पंचवर्षीय योजनाएं भारत के विकास की रीढ़ रही हैं। इन्होंने कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना जैसे क्षेत्रों में देश को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यद्यपि अब ये योजनाएं बंद हो चुकी हैं, लेकिन इनके अनुभवों से वर्तमान नीति निर्माण को दिशा मिलती है।